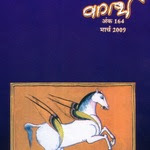केदारनाथ सिंह की 61 कविताओं का संग्रह 'अकाल में सारस' 1988 में आया जिसमें सन् 1983 से 1987 तक की कविताएं संकलित हैं। इस संग्रह में उनकी कविताओं की उत्कष्टता पहले से बढ़ी है और कथ्य तथा रूप दोनों ही स्तरों पर इसमें उल्लेखनीय परिवर्तन घटित हुए हैं। पहले से परिवक्व पहले से अधिक प्रभावी। अर्थ परिवर्तन की जो प्रक्रिया उनमें शुरू हुई थी लगता है कि यही वह गंतव्य है जहां वे पहुंचना चाहते थे। उनका व्यक्तिगत जीवन, विश्व साहित्य का सतत अध्ययन और समूचा विश्व होना चाहने की चाहत यहां एक ऐसी काव्य दृष्टि का विकास करने में सक्षम हुई है जो हिन्दी व भारतीय कविता में किसी हद तक विरल है। इस संग्रह में मनुष्य की अक्षय उर्जा व अदम्य जिजीविषा है और परम्परा से मिली दिशाएं हैं जिनका संधान उन्होंने आवश्यकतानुसार अपनी पिछली ज़िन्दगी की ओर मुड़कर भी किया है। वे अपने काव्य सृजन में आगे तो बढ़ते रहे हैं किन्तु पीछे का नष्ट नहीं करते बल्कि उसकी भी कोई न कोई लीक बची रहती है जहां आवश्यकतानुसार वे लौटते हैं। कवि केदार कविता के नये अनजान सफर पर बार-बार जाते हैं तो वहां पीछे छूटा हुआ बहुत कुछ भी काम का लगता है और वे पीछे छूटे हुए को भी आगे की यात्रा का पाथेय बना लेते हैं। 'केदारनाथ सिंह ने फिर कुछ पुरानी लयों पर पुनर्जीवित किया है। एक कविता निराला को याद करते हुए उन्हीं की ज़मीन पर लिखी गयी है।' ( कमल, अरुण, कवि केदारनाथ सिंह, पृष्ठ 223) भौतिक रूप से वे महानगर में हैं तो मानसिक रूप में लोक की ओर पहले से अधिक आकृष्ट हुए हैं। उन्हें इस बात का लगातार एहसास होता रहा है कि लोक -जीवन ही उनकी काव्य-भूमि और मनोभूमि है जिसे लेकर उन्हें दिगंत पार जाना है। जड़ों की ओर लौटना ही उनमें ऊर्जा का संचार करता है और ताज़गी भरता है। वे अपने साथ कुछ सूत्र लेकर बढ़े हैं और समय आने पर उन्हें गुनते हैं जो उन्हें असंजस से उबारता है और दिग्भ्रमित नहीं होने देता। आधुनिकता के देशज स्वरूप का विकास वे शुरू से धीरे-धीरे कर रहे थे और वह नयी ऊंचाइयों तक जाता है। पहली की कविता में वे इस संग्रह की उस बात को कहते हैं जो इसकी केन्द्रीय धुरी है। इसके पहले भी उनके कतिपय काव्य संग्रहों में पहली कविता ने पुस्तक की भूमिका का कार्य किया है। इसमें वे कहते हैं-
'जैसे चीटियां लौटती हैं
बिलों में
कठफोड़वा लौटता है
काठ के पास
वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक
लाल आसमान में डैने पसारे हुए
हवाई अड्डे की ओर
ओ मेरी भाषा
मैं लौटता हूं तुम में
जब चुप रहते-रहते
अकड़ जाती है मेरी जीभ
दुखने लगती है
मेरी आत्मा।' (सिंह, केदारनाथ, अकाल में सारस, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 1988, मातृभाषा, पृष्ठ 11)
यह जो मेरी भाषा का जिक़्र है वह केदार की वह लोक भूमि है जहां उनकी रचनात्मकता का अजस्र स्रोता है। जितना ही वे अपनी जड़ो की ओर लौटते हैं बाह्य संसाकर का भी उसी अनुपात में विस्तार होता जाता है।
यहीं केदार जी की उस बीस वर्ष की चुप्पी का राज भी खुलता है जो 'अभी बिल्कुल अभी' से 'ज़मीन पक रही है' के बीच है। रचनाशीलता उनके लिए अपनी भाषा के पास लौटना है और व्यवस्था के ख़िलाफ चुप्पी उनके प्रतिकार का अन्दाज़। साठोत्तरी दौर में जब कवियों के कई-कई संग्रह निकल रहे थे और शिल्प व कथ्य को लेकर नित नये आंदोलन छिड़े थे उन्होंने चुप्पी की शरण ली थी। केदार जी के यहां अस्वाभाविक परिस्थितियों में रचनाशीलता सम्भव नहीं है। वे तब लिखते हैं 'जब चुप रहते-रहते अकड़ जाती है जीभ, दुखने लगती है आत्मा।' (वही)
केदार जी के प्रकृति का भयावह रूप और विभीषिका प्रायः नहीं है। किन्तु इस संग्रह में अकाल पर उनकी दो कविताएं हैं शीर्षक कविता 'अकाल में सारस' और 'अकाल में दूब'। अकाल पर केदार जी के अग्रज कवि नागार्जुन ने 'अकाल और उसके बाद' तथा समकालीन कवि रघुवीर सहाय ने 'अकाल' कविता लिखी है। अकाल से जन जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को ही इन कवियों ने चित्रित किया है। विषय वस्तु एक होते हुए भी अकाल पर इन तीनों कवियों का भावबोध अलग है और तीनों का अपना-अपना विशिष्ट अन्दाज़ है और वस्तुजगत पर प्रतिक्रिया की अपनी शैली, अपनी भाषा। नागार्जुन अकाल के बाद के सामान्य जीवन से अकाल की स्थितियों की भयावहता को उभारते हैं तो रघुवीर सहाय अकाल के जिम्मेदार कारकों के प्रति गंभीर हैं।
केदार जी की अकाल पर लिखी दोनों कविताओं में उनकी नाटकीय शैली विद्यमान है। 'अकाल में दूब' में पूरा दृश्य एक समारोह जैसा। चित्र और स्थितियां बोलती हैं मंत्रणा करती हैं और अकाल में यदि दूब बची है तो जीवन की आशा भी बची है के निष्कर्ष तक कविता पाठक को पहुंचाती है। यह जीवन की वह कुंजी है जिस तक केदार जी की कई कविताएं पहुंचतीं है पहुंचाने की कोशिश करती हैं। 'अकाल में सारस' कविता में सुदूर प्रदेशों से सारस पानी की तलाश में आते हैं। एक बुढ़िया अपने आंगन में एक जलभरा कटोरा रखती है। सारस उस कटोरे को देखते तक नहीं और उड़ जाते हैं। एक पूरा दृश्य। एक फ़िल्म की पटकथा सी गतिविधियों की बारीक से बारीक घटना दर्ज़ है। 'केदार वर्णन नहीं चित्रण करते हैं। प्रायः उनकी संवेदना देखे हुए को किसी शॉट की तरह कम्पोज़ करने के करीब पहुंचने लगती है। (प्रसाद, गोविन्द, मिट्टी की रोशनी, सम्पादकः त्रिपाठी, अनिल,शिल्पायन, दिल्ली,2007, पृष्ठ 105)
दरअसल यह कविता भौतिक अर्थ में अकाल पर होते हुए भी अर्थ के अतिक्रमण की कविता है और वह शहर को दया या घृणा का पात्र मानने की टिप्पणी के साथ ख़त्म होती है। शहर में जीवन तत्त्व पानी की उपलब्धता के बारे में सारसों के अनुमान को वे यूं बयां करते हैं-
'पानी को खोजते
दूर-देसावर तक जाना था उन्हें
सो, उन्होंने गर्दन उठाई
एकबार पीछे की ओर देखा
न जाने क्या था उस निगाह में
दया कि घृणा
पर एक बार जाते-जाते
उन्होंने शहर की ओर मुड़कर
देखा ज़रूर।'
(अकाल में सारस/ पृष्ठ 23)
हालांकि इस कविता में भी केवल निराशा नहीं है। संकेत है-
'अचानक
एक बुढ़िया ने उन्हें देखा
ज़रूर ज़रूर
वे पानी की तलाश में आये हैं
उसने सोचा
वह रसोई में गयी
और आंगन के बीचोबीच
लाकर रख दिया
एक जलभरा कटोरा।'
बुढ़िया का पानी की तलाश में आये सारसों के लिए जलभरा कटोरा रखना ही अकाल में दूब की स्थिति है। यहां संवेदना के अकाल की स्थिति में दूब है। 'लोक संवेदना में अकाल के दिनों में दूब पानी का, जीवन का, प्राण तत्त्व का पर्याय है।'(रोहिताश्व, मिट्टी की रोशनी, सम्पादकः त्रिपाठी, अनिल,शिल्पायन, दिल्ली,2007, पृष्ठ 74) 'अकाल में दूब' कविता में इसकी बानगी देखें-
'कहते हैं पिता
ऐसा अकाल कभी नहीं देखा
ऐसा अकाल कि बस्ती में
दूब तक झुलस जाय
सुना नहीं कभी
x x x x x x x x x
अचानक मुझे दिख जाती है
शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच
एक हरी पत्ती
दूब है
हां-हां दूब है-
पहचानता हूं मैं
लौटकर यह खबर
देता हूं पिता को
अंधेरे में भी
दमक उठता है उनकी चेहरा
है-अभी बहुत कुछ है
अगर बची है दूब।'
(अकाल में दूब, अकाल में सारस, पृष्ठ 20/21)
पहली नज़र में किसी को लग सकता है कि विषय वस्तु के चयन के लिहाज़ से ये कविताएं यथार्थपरक होते हुए भी वह अन्ततः कलारूप को ही अधिक तरज़ीह देती प्रतीत होती है, किन्तु ऐसा है नहीं। दरअसल बाह्य उपकरणों, कवि के औज़ारों को ही कथ्य मान लेने से ऐसा भ्रम होता है केदार जी के यहां वस्तु जगत एक भाव जगत तक ले जाने का माध्यम है यहां भी ऐसा ही हुआ है। दूसरे कवि का वस्तु जगत के प्रति गहरा लगाव, उसके स्वभाव और व्यवहार के प्रति गहन अध्ययन और चिन्ता यह भ्रम पैदा कर देता है कि वही मुख्य अभिप्रेय हैं उपादान नहीं। केदार जी ने अपने कथ्य को प्रभावी बनाने के लिए अकाल में सारस कविता में फ़ेटेसी का सहारा लेते हैं। यही कारण है कि विनोद दास जैसे कवि आलोचक लिखते हैं 'अकाल के भयावह और जटिल यथार्थ रूपों के अन्वेषण के बजाय इस कविता के विन्यास में एक रोमानी नाटकीयता अन्तर्निहित है। पूरा प्रसंग एक समारोह सदृश्य लगता है। शब्दमोह और चित्रमोह के चलते वास्तविकता पर कवि की पकड़ ढीली पड़ जाती है। दरअसल यह कवि की भाव-बोध की दुर्बलता है।' (कविता यही करती है, दास, विनोद, पहल पुस्तिका/अंक-37, 763, अग्रवाल कालोनी, जबलपुर, पृष्ठ 39)
इन दोनों कविताओं के बारे में रोहिताश्व की टिप्पणी इन दोनों कविताओं के मर्म के अधिक करीब पड़ती हैं-'अकाल में दूब कविता विपरीत स्थितियों में, सूखे अकाल की स्थिति में दूब के अगर बचे रहने की गवाही देती है तो यह अकाल की विषमता के समानान्तर आशा-विश्वास और जीवन सौन्दर्य की अनुभूति है, यहां नश्वरता के बरक्स अनश्वरता का सौन्दर्यबोध गतिशील है। वस्तुतः 'अकाल में सारस' मानवीय विसंगतियों को रेखांकित करने वाला ऐन्द्रिय जगत की संवेदना के ख़ात्मों का वह सौन्दर्यबोधी परिदृश्य है जो हमें उस अभाव की पूर्ति हेतु मनुष्यता और रागात्मकता की सक्रियता अपनाने का संदेश देता है।' (रोहिताश्व, मिट्टी की रोशनी, सम्पादकः त्रिपाठी, अनिल,शिल्पायन, दिल्ली,2007, पृष्ठ 76)
'अकाल और सारस' में जीवन और मृत्यु को लेकर कई कविताएं हैं जो कैंसर से जूझती उनकी पत्नी के संदर्भ से जुड़ी होने के कारण आत्मपरक होते हुए भी अपने शिल्प व कथ्य के वैशिष्ट के चलते उतनी ही सार्वजनीन भी हैं। इन कविताओं में मृत्यु के पंजा लड़ाती अड़ियल सांस है और जीवन मृत्यु को लेकर कवि के मन में गहराई से उठते प्रश्न व उनका सामना करने का जीवट। कुछ कविताएं प्रत्यक्ष है तो कुछ में परोक्ष रूप से जीवन-मृत्यु के प्रश्नों से जुड़ी हुई। न होने की गंध, अड़ियल सांस, पर्वस्नान, सूर्यास्त के बाद एक अंधेरी बस्ती से ग़ुजरते हुए, लोककथा जैसी कविताओं के केन्द्र में मृत्यु भी है। मृत्यु के बाद एक टीस न होने की गंध में तब्दील हो जाती है-
'सबसे अधिक खाली थे हमारे कंधे' (न होने की गंध, अकाल में सारस, पृष्ठ45)
इसके लिए बस्ती में एक गहरी उदासी थी
'यों हम लौट आये
जीवितों की एक लम्बी उदास बिरादरी में' (न होने की गंध, अकाल में सारस, पृष्ठ46)
अभाव को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने होने को न होने और न होने को होने में तब्दील कर दिया है-
'कुछ नहीं था
सिर्फ़ कच्ची दीवारों
और भीगी खपरैलों से
किसी के न होने की
गंध आ रही थी'(न होने की गंध, अकाल में सारस, पृष्ठ 46)
इन कविताओं में स्थितियों का वर्णन है, जो स्थिति की तल्खी को शिद्दत से महसूस करने पर पाठक को विवश कर देता है। 'केदारनाथ सिंह चीज़ों का वर्णन ठीक-ठीक करने वाले हिन्दी के विरले कवियों में से हैं और चीज़ों का ठीक-ठीक वर्णन जहां एक ओर सौन्दर्य और उल्सास की ओर ले जाता है वहां जीवन की विसंगतियों, एब्सर्डिटीज की ओर भी ले जाता है।' (विष्णु खरे, कवि केदारनाथ सिंह, पृष्ठ 240)
मृत्यु के सवालों से इस संग्रह में वे बेतरह जूझते हैं। ज़्यादातर पत्नी की मृत्यु पर लिखी इस संग्रह की कविताओं के क्रम में ही वे अपने जीवन के बारे में सोचते हैं जिसमें मृत्यु की बात प्रकारांतर से विद्यमान है। मृत्यु के सम्बंध में खयाल जीवन के खयाल से परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है किसी के लिए मृत्यु क्या है यह जानने के लिए यह जानना कम नहीं है कि उसके लिए जीवन क्या है-
'मेरा जीवन
एक दोना है
सींक से बुना हुआ पत्तों का दोना
जिसमें मेरे जन्म के दिन से ही
टप् टप् टपक रही है धूप
मैं उसे पीता हूं
और जितना पीता हूं
उतना ही बूंद-बूंद भरता जाता है मेरा दोना
दोना ही तो है
कोई एक दिन उठाकर फेंक देगा बाहर
पर उसी को लेकर अपने दोनों हाथों में
मैं सूर्य से भी ज़्यादा सम्पन्न हूं
इस पृथ्वी पर।' (जन्म दिन की धूप में, अकाल में सारस, पृष्ठ 64-65)
केदार जी के लिए सूर्य से भी अधिक सम्पन्न होने की बात है इसलिए मृत्यु उन्हें अधिक त्रासद और ससह्य है। विपन्नकारी।' मृत्यु की चेतना, ज़िन्दगी के तिल-तिल को सम्भाल कर-जुगा कर जीने की उत्कट लालसा, उनकी अनेक कविताओं में देखने को मिलती है।' (सिंह, भगवान, कवि केदारनाथ सिंह, पृष्ठ 77)
जीवन मृत्यु से जुड़ी एक और कविता है इस संग्रह में 'एक दिन भक् से'-
'एक दिन भक् से
मूंगा मोती
हल्दी प्याज
कबीर निराला
झींगुर कुहासा
सभी के आशय स्पष्ट हो जायेंगे
जैसे धूप
खपरैलों पर
जाते-जाते यकायक
स्पष्ट हो जाती है।' (एक दिन भक् से,सिंह केदारनाथ, अकाल में सारस, पृष्ठ 83)
लोकमान्यता है कि मृत्यु के पूर्व किसी व्यक्ति को सब कुछ साफ-साफ दिखायी देने लगता है सारे आशय स्पष्ट हो जाते हैं। इसी मनोभूमि पर एक कालजयी कृति सी, टहलते हुए बूढ़े कविताओं भी हैं जिनमें जीवन मृत्यु के प्रश्न विद्यमान हैं।
हालांकि मृत्यु को स्वाभाविक तौर पर स्वीकारने का प्रयास भी उन्होंने किया है। प्रकृति की अन्य स्वाभाविक प्रक्रियाओं में से मृत्यु को एक मानने की उपक्रम दीखता है-
'जैसे आकाश में तारे
जल में जलकुम्भी
हवा में आक्सीजन
पृथ्वी पर उसी तरह
मैं
तुम
हवा
मृत्यु
सरसों के फूल।' (फलों में स्वाद की तरह, अकाल में सारस, पृष्ठ 15)
इन पंक्तियों में मृत्यु का दंश नहीं है। मृत्यु के सम्बंध में दर्शन है जो अन्य को समझाने के उपक्रम में रचा प्रतीत होता है। 'मृत्यु' के बाद 'सरसों का फूल' लिखकर उन्होंने मृत्यु जैसे गंभीर मसले को प्रकृति की साधारण और अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा बनाने का प्रयास किया है। कोई भी स्थिति असह्य नहीं है। प्रिय अप्रिय सब समान भाव से ग्रहण करने की मनःस्थिति का द्योतक है। इस कविता में आगे वे लिखते हैं-
'जैसे दियासलाई में काठी
घर में दरवाज़े
पीठ में फोड़ा
फलों में स्वाद
उसी तरह
उसी तरह।' ( (फलों में स्वाद की तरह, अकाल में सारस, पृष्ठ 15)
पीड़ा को स्वाभाविक बनाने की प्रयास यहां भी है वरना 'पीठ में फोड़ा' जैसी अस्वाभाविक स्थिति को 'फलों में स्वाद' जैसी स्वाभाविक स्थिति के क्रम में नहीं जोड़ते। पीठ में रीढ़ स्वाभाविक है किन्तु फोड़ा नहीं। साफ़ पता चलता है कि असामान्य स्थितियों को भी वे सामान्यकृत करने का प्रयास कर रहे हैं।' केदारनाथ सिंह दो विपरीत संवेगों, दृश्य चित्रों और भावानुभूतियों को परिवेशगत तनाव में रचते हैं।' (रोहिताश्व, मिट्टी की रोशनी, सम्पादकः त्रिपाठी, अनिल,शिल्पायन, दिल्ली,2007, पृष्ठ 61)
केदार जी जीवन मृत्यु के प्रश्नों पर विचार करते समय केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं रह जाते। वे एक कवि के पुनर्जन्म ही नहीं, बल्क़ि वस्तुओं के पुनर्जन्म के बारे में भी सोचते हैं-
'लेकिन प्रिय पाठक
एक कवि का काम चलता नहीं है
अगले जनम के बिना
वह यही तो करता है अधिक से अधिक
कि लोगों में
यहां तक कि चीज़ों में भी
हमेशा बनी रहे
बार-बार जनम लेते रहने की इच्छा।' (प्रिय पाठक, सिंह केदारनाथ, अकाल में सारस, पृष्ठ 108)
मृत्यु के साक्षात की स्वाभाविक कविता है 'सूर्यास्त के बाद एक अंधेरी बस्ती से गुज़रते हुए'-
' भर लो
ताकती हुई आंखों का
अथाह सन्नाटा
सिवानों पर स्यारों के
फेंकरने की आवाज़ें
बिच्छुओं के
उठे हुए डंकों की
सारी बेचैनी
आत्मा में भर लो।'
x x x x x x x x x x x x x x x
इससे पहले कि भूख का हांका पड़े
और अंधरा तुम्हें चीथ डाले
भर लो
इस पूरे ब्रह्मांड को
एक छोटी सी सांस की डिबिया में भर लो।'
(सूर्यास्त के बाद एक अंधेरी बस्ती से गु़जरते हुए, अकाल में सारस, पृष्ठ 17)
भूख यहां पर मृत्यु है। मृत्यु को सम्मुख पाकर जीवन के प्रति गहरी आसक्ति और प्रबल हो उठती है।-'अकाल में सारस की उन कविताओं में जिनमें कवि अपनी परिचित और आत्मीय दुनिया में वापस आता हुआ दिखायी पड़ता है वे कविताएं निःसंदेह कवि की सबसे सुन्दर कविताएं हैं और आज के दौर की स्मरणीय कविताएं। x x x x x x x x अकाल में सारस में इसी शीर्षक की कविता को मिलाकर ऐसी अनेक कविताएं हैं जिनमें केदार जी बार-बार मुड़कर अपने काव्य उपकरणों, आधारों और बिम्बों की ओर लौटते हुए दिखायी देते हैं, जो उनकी पहले की कविताओं में भी मौज़ूद है।x x x x x x x x इसका अर्थ यह नहीं है कि केदार जी इन कविताओं में कहीं पीछे की ओर लौटते हैं और वहीं ठहरे हुए रहना चाहते हैं बल्क़ि इसका अर्थ यह है कि वे इन आधारों को मज़बूती से थामे हुए जीवन के नये अर्थों को आविष्कृत करते हैं।' (कुमार, सुरेश, कवि केदारनाथ सिंह, पृष्ठ134)
इस संग्रह से गुज़रकर पाठक को कवि केदारनाथ सिंह का एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो आगे की राह तो पुख्ता करता है किन्तु पीछे छूटे अपने महत्त्वपूर्ण आधारों पर अपनी पकड़ पहले की अपेक्षा मज़बूत करता चलता है वापसी का कवि कहे जाने का ज़ोखिम उठाते हुए भी। कवि का आत्मसंघर्ष अपेक्षाकृत तेज़ हुआ है और उसमें रूप और वस्तु के प्रति आश्वस्ति का बोध कम हुआ है। पिछले संग्रह में उसका जो स्वर मुखर हुआ था अब वह संयत हो चुका है। दूसरे जीवन-मुत्यु के संघर्ष इसका लगभग मूल स्वर बना है जो पहले नहीं था। गांव के जीवन के प्रति उसका लगाव बना हुआ है किन्तु उसका स्वरूप बदला है। इस सम्बंध में उसकी रुमानियत कम हुई है किन्तु लगाव नहीं। अरुण कमल ने ठीक कहा है-'गांव और गांव के सन्दर्भ बिल्कुल नये ढंग से इन कविताओं में आये हैं। गांव पर लिखी कविताएं प्रायः आंचलिक हो जाती हैं, स्वयं भी ग्रामीण लगने लगती हैं। साथ ही साथ एक प्रकार के मोह का भाव भी यहां रहता है। गांव का जीवन प्रायः नॉस्टेल्जिया के साथ कविता में आता है। केदारनाथ सिंह ने इन कविताओं के जरिये गांव को एक नये ढंग से, आधुनिक तरीक़े से देखने की कोशिश की है। संभवतः यह ऐसी पहली महत्त्वपूर्ण कोशिश है। इसीलिए उनके गांव पुराने तरह के पारम्परिक गांव नहीं हैं जिनकी स्तुति हिन्दी कविता ने निरन्तर की है। यहां गांव का जीवन कोई पृथक् निर्दोष जीवन नहीं है-कोई स्वायत्त अंचल नहीं है। यह शेष सम्पर्ण जीवन में ही प्रशस्त है। वास्तव जीवन में एक ही है-एक ही पीड़ा और संघर्ष का विस्तार। 'सूर्यास्त के बाद एक अंधेरी बस्ती से ग़ुजरते हुए' के उपर्युक्त पाठ से यह स्पष्ट है। इन कविताओं की सबसे बड़ी ख़ूबी है-आंचलिकता से मुक्ति।' (कमल, अरुण, कवि केदारनाथ सिंह, पृष्ठ 218)
यहां इस सदर्भ में यह और जोड़ना ठीक रहेगा कि गांव हो या शहर प्रकृति के प्रति उनका अनुराग बरकार है और उसका भी विस्तार हुआ है नयी अर्थ सघनता आयी है। प्रकृति के क्रिया कलापों के बाह्य चित्रण के साथ-साथ वे उसके आन्तरिक गुणों से भी जुड़ते नज़र आते हैं। वे फल से उसका स्वाद तक पहुंचे हैं। अब वे मनुष्य के प्रकृति के रिश्ते तो शिद्दत से महसूस करते हैं। 'नये शहर में बरगद' को वे अपने घर चाय पर ले जाना चाहते हैं। बालू का स्पर्श उन्हें रोमांचित करता है। प्रकृति का सहज साहचर्य और उसके आनंद को भी उन्होंने इस संग्रह में पर्याप्त स्थान दिया है-
'अच्छा लगा बालू का स्पर्श
बहुत-बहुत अच्छा लगा
सोचता रहा देर तक
आख़िर छोटे-छोटे कणों की लहक
और छटपटाहट के अलावा
क्या है
क्या है बालू में
जो आदमी को कर दे
इतना विभोर।' (बालू का स्पर्श, सिंह केदारनाथ, पृष्ठ 38-39)
संग्रह में 'चिट्ठी' कविता में अपने गांव चकिया को याद करते हैं तो 'आंकुसपुर' स्टेशन पर ट्रेनों के न रुकने की कसक उन्हें सालती है। 'कुछ सूत्र जो एक किसान बाप ने बेटे को दिये' कविता में जीवन के मर्म भी हैं और उनकी कविता की प्रतिबद्धताएं भीं, जो उनकी लोकसम्पृक्ति को प्रकट करती हैं।
'अकाल में सारस' में 'बाजार एक तकलीफ़देह संदर्भबिन्दु के मानिन्द उनके इस कविता संग्रह में बार-बार उभरता है।'(चतुर्वेदी, पंकज, मिट्टी की रोशनी, सम्पादक, त्रिपाठी, अनिल, शिल्पायन, दिल्ली,2007, पृष्ठ 139) बाज़ार और आदमी के रिश्ते पर पिछले संग्रहों में भी उनकी कविताएं थीं किन्तु इस रिश्ते पर उन्होंने फिर गंभीर दृष्टि डाली है। एक छोटा सा अनुरोध, दाने, पशुमेला आदि कविताएं बाज़ार पर लिखी गयी हैं। वे बाज़ार को दरकिनार करने के हिमायती रहे हैं। वे कहते हैं-
कैसा रहे
बाज़ार न आये बीच में
और हम एक बार
चुपके से मिल आयें चावल से
मिल आयें नमक से
पुदीने से।(एक छोटा सा अनुरोध, पृष्ठ14)